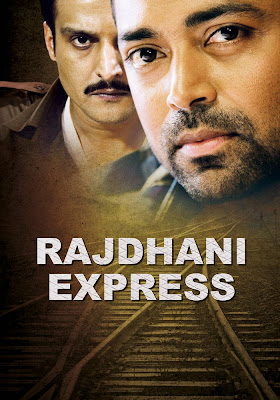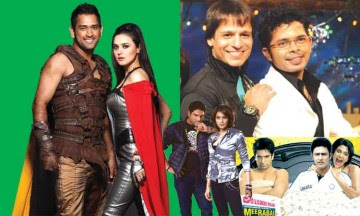एक दौर था, जब टेनिस की दुनिया में भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं था. अमृतराज के अलावा टेनिस में शायद ही कोई नाम हो, जिसकी वजह से भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय खेल परिदृश्य में उभरा हो. व़क्त गुजरा और सानिया एवं साइना ने टेनिस वर्ल्ड में पदार्पण किया. इनके क़दम रखते ही ग्लैमर ने भी इस खेल में ज़बरदस्त घुसपैठ की. ग्लैमर के तड़के ने सानिया मिर्जा को तो अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन साइना अभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर हैं. न स़िर्फ बाहर है, बल्कि उनका प्रदर्शन भी दिनोंदिन बेहतर होता जा रहा है. खेल के कई बड़े पुरस्कारों से नवाजी जा चुकीं 20 वर्षीय साइना इस समय भारत की सबसे सफल महिला खिलाड़ी हैं. जिस तरह उन्होंने हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन खिताब अपने नाम कर एक बार फिर विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में दूसरे पायदान पर जगह बनाई है, वह काबिले तारी़फ है. ग़ौरतलब है कि साइना हांगकांग टूर्नामेंट से पहले दो स्थान गिरकर चौथे स्थान पर पहुंच गई थीं, लेकिन फिर से हांगकांग के एक कड़े मुक़ाबले मेंबाज़ी मारकर उन्होंने अपनी रैंकिंग में दो स्थान का सुधार किया और फिर से दूसरे पायदान पर पहुंच गईं. बीते साल के बेहतर प्रदर्शन को बरक़रार रखते हुए उन्होंने 2010 में पांच खिताबों और देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न को अपनी झोली में डाला.
लेकिन यहां ग़ौर करने वाली बात यह है कि उन्हें यह सफलता यूं ही नहीं मिल गई है. इस सफलता की कहानी लिखने में कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष की स्याही छिपी हुई है. 17 मार्च, 1990 को हरियाणा के हिसार में जन्मी साइना आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में पली-बढ़ी हैं. उनका बैडमिंटन प्रशिक्षण सात साल की उम्र में ही हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में शुरू हो गया था. उनके माता-पिता भी हरियाणा की तऱफ से बैडमिंटन खेलते थे. ज़ाहिर है, उनके असर से साइना अछूती नहीं रहीं. वह कहती हैं कि मेरे माता-पिता ने मुझे एक बेहतर खिलाड़ी बनाने में जितनी मेहनत की है, अच्छे प्रदर्शन के बल पर वह उसे सफल करना चाहती हैं. ग़ौरतलब है कि साइना के पिता हरवीर सिंह हैदराबाद के डायरेक्ट्रेट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च में वैज्ञानिक हैं. पिता हरवीर सिंह के मुताबिक़, साइना जिस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाती थी, वह घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था. ट्रेनिंग सेशन के बाद साइना को स्कूल भी जाना होता था. ऐसे में मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने और ले आने के लिए 50 किलोमीटर स्कूटर चलाकर जाता था. बीते दिनों को याद करते हुए वह कहते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन शुरू होने के बाद हर दिन साइना पर 150 रुपये का ख़र्च गाड़ी-भाड़ा पर आता था. इसके अलावा रैकेट एवं जूते आदि ख़रीदने पर भी ख़र्च होता था. इस तरह हर महीने उस पर 12 हज़ार रुपये ख़र्च होने लगे. चूंकि उस समय इतनी बड़ी राशि ख़र्च करना मेरे लिए मुश्किल था, सो इस ख़र्चे को मैनेज करने के लिए मुझे अपने प्रॉविडेंट फंड से पैसे भी निकालने पड़े. कभी-कभी साइना की खेल संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए 30 हज़ार रुपये तो कभी एक लाख रुपये तक निकालने पड़े. इसी तरह न जाने कितने संघर्ष के रास्तों से गुजर कर साइना इस मुक़ाम तक पहुंची है.
हालांकि साइना अभी अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर हैं. उनका अंतिम लक्ष्य विश्व रैंकिंग में एक नंबर के पायदान पर पहुंचना है. अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो साइना ने 2006 में विश्व बैडमिंटन जगत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी. यह वह दौर था, जब उन्होंने फिलीपींस ओपन प्रतियोगिता जीती. बीजिंग में आयोजित ओलंपिक खेलों में वह अंतिम आठ में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी भी बनी थीं. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तबसे अभी तक विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ती जा रही हैं. हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं. इन चुनौतियों में कड़ी प्रतियोगिताएं हैं, साथ ही सफलता का गुरूर, ग्लैमर की चकाचौंध और पेज थ्री पार्टियां भी हैं. अगर इन सबसे साइना बची रहती हैं तो फिर खेलप्रेमियों का आशीर्वाद और उम्मीदें उनके साथ हैं.
साइना में ओलंपिक मेडल जीतने की क्षमता है. उसने अभी अपना करियर ही शुरू किया है. वह कम से कम दो और ओलंपिक में हिस्सा लेगी. दिनोंदिन उसका खेल और धारदार होता जा रहा है.
-पी गोपीचंद, साइना के कोच एवं पूर्व बैडमिंटन चैंपियन
साइना कई वर्षों से किसी पार्टी, रेस्तरां या सिनेमाहॉल में नहीं गई थी. जब पहली बार मीडिया वाले मेरे घर पर एक कार्यक्रम शूट करने आए तो मैं मिठाई भी नहीं खिला सका.
-हरवीर सिंह, साइना के पिता